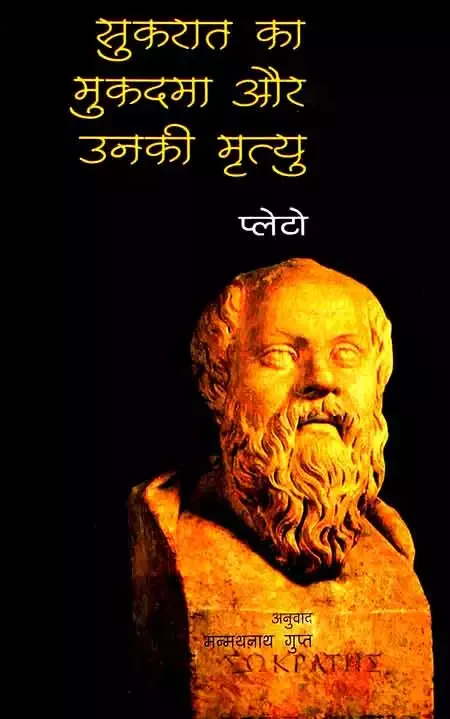|
जीवनी/आत्मकथा >> सुकरात का मुकदमा और उनकी मृत्यु सुकरात का मुकदमा और उनकी मृत्युप्लेटो
|
97 पाठक हैं |
|||||||
ग्रीक दार्शनिक सुकरात के लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व दिये वक्तव्यों और मान्यताओं का वर्णन...
Sukrat Ka Mukadama Aur Unaki Mrityu - A Hindi Book - by Plato
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
आज हम जिसे यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के नाम से जानते हैं, उसमें निश्चित रूप से ग्रीस का सबसे अधिक दान है। यों तो यह कहा जाता है कि यूरोप ने रोमनों से कानून की एक महान पद्धित तथा उसके साथ ही साथ राज्य-संचालन का कौशल प्राप्त किया, जूडिया से धर्म पाया और ग्रीस से दर्शन, विज्ञान और साहित्य पाया, पर इतने से सत्य प्रकट नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों के बड़े से बड़े साहित्यकारों ने ग्रीस की बात छिड़ते ही जिस उच्छ्वसित ढंग से उसकी प्रशंसा की है, वह बहुत ही विशिष्ट है।
हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार जर्मन महाकवि गेटे ने कालिदास के शकुंतला नाटक की प्रशंसा की है, पर ग्रीस के कवियों के संबंध में उनके ये मंतव्य विशेष ध्यान देने योग्य हैं। उनका कहना है : ‘‘इशीलस और सोफोक्लिस की तरह प्राचीन ग्रीक कवियों के सामने मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूं।’’
कवि वर्डसवर्थ ने इसी प्रकार कहा है : ‘‘भला डिमोस्थिनिस से बढ़कर वक्ता और शेक्सपियर के बाद इशीलस-सोफोक्लिस (यूरिपिडिस का तो कुछ कहना ही नहीं) के मुकाबले में काव्यमय नाटक कहां मिल सकते हैं ।’’
हेरोडोटस से संबंध में वर्डसवर्थ का यह कहना था कि बाइबिल के बाद उससे बढ़कर दिलचस्प और शिक्षाप्रद कोई पुस्तक नहीं है। कविवर शैली की प्रशंसा इनके मुकाबले में कम उच्छ्वसित थी, पर उनका भी यह कहना था : ‘‘ग्रीकों की कविता दूसरे साहित्यों के मुकाबले में काफी ऊंचा मानदंड रखती है, यद्यपि वह इतनी ऊंची नहीं है कि वह बहुत ऊंची जंचे और दूसरी बहुत नीचे।’’
उनका कहना था, ‘‘पैरिक्लिस के जन्म और अरस्तू की मृत्यु के बीच का युग निश्चित रूप से विश्व-इतिहास का सबसे स्मरणीय युग है। चाहे इस पर अलग से विचार किया जाए या बाद के सभ्य मानव पर उसका क्या असर रहा, उस दृष्टि से उस पर विचार किया जाए।... इन सूक्ष्म और गंभीर मनों के जो इतस्ततः विक्षिप्त टुकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, वे सुंदर मूर्ति के भग्नांशों की तरह हमारे सामने अस्पष्ट रूप से उस समय की महत्ता तथा पूर्णता का चित्र पेश करते हैं जो अब नहीं रहा। विविधता, सरलता, नमनीयता, प्रचुरता, जिस दृष्टि से भी देखा जाए, पाश्चात्य जगत में ग्रीक भाषा से बढ़कर कोई भाषा न रही।’’
इसी प्रकार सैकड़ों उद्धरण दिए जा सकते हैं। फ्रांस के युगांतरकारी लेखक अनातोल फ्रांस का यह वक्तत्व्य सुनिए : ‘‘मैं अब जानता हूं कि मैं ग्रीकों का कितना ऋणी हूं क्योंकि मेरा सब कुछ उन्हीं का है। हम जानते हैं जगत और मनुष्य का जो कुछ भी बुद्धिसंगत है, वह सब उन्हीं से आया हुआ है।’’
मिल का तो यह कहना था कि ईसाइयत के अतिरिक्त बाकी सभी ऐसी चीजों की उत्पत्ति, जिन पर आधुनिक जगत नाज करता है, ग्रीस से हुई। और उद्धरणों को आवश्यकता नहीं है।
हम सुकरात के पहले के ग्रीक दर्शन-शास्त्र पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें। थेलस या थेलिस को ग्रीक दर्शन का पिता बताया गया है। उनका जन्म ई. पू. 626 में एशियाई कोचक के मिलिटस नामक स्थान में हुआ था। इनका कहना था कि जल ही मौलिक उपादान है और उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि आर्द्रता एक ऐसा उपादान है, जो सब में परिव्याप्त है। इस प्रकार से वे भौतिकवादी थे, क्योंकि वे जल से ही जगत की उत्पत्ति मानते थे। मजे की बात यह है कि वे देवताओं को भी मानते थे, पर साथ ही यह भी बताते थे कि उत्पत्ति भी जल से ही हुई है।
ऐनैक्सिमिनिस नामक दार्शनिक भी मिलिटस में पैदा हुए थे। उनका जन्म ई. पू. 529 या ई. पू. 548 में हुआ। वे सब चीजों की उत्पत्ति वायु से मानते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके अंदर जो वायु है, वही उन्हें चला रही है और यही जीवन है। उन्होंने इस प्रकार तर्क किया कि भीतर की वायु बाहर की वायु का ही अंग है, इसलिए सब चीजों की उत्पत्ति वायु से ही हुई। इस प्रकार ऐनैक्सिमिनिस भी भौतिकवादी रहे।
पर उनके अनुयायी ऐपोलोनिया के डोयोजिनिस ने एक नया मोड़ दिया और भाववाद का प्रारंभ किया। डोयोजिनिस ने ऐनैक्सिमिनिस के अनुसार वायु को ही प्रथम माना। पर उन्होंने वायु को एक विस्तृतर और गंभीरतर अर्थ दिया, जिसमें वह करीब-करीब आत्मा हो गयी। उन्होंने इसे शक्ति और बुद्धि से समन्वित करके कल्पना की। उन्होंने यह भी कहा कि यह विश्व एक सप्राण अस्तित्व है, जो स्वतःस्फूर्त रूप से अपना विकास कर रहा है और इसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, वह उसकी जीवनी-शक्ति के कारण हो रहा है।1 उनका कहना यह था कि सारी सृष्टि और पादार्थिक क्रिया श्वास-प्रश्वासमूलक है। उन्होंने आर्द्रता के प्रति सूर्य के आकर्षण और लोहे के प्रति चुंबक के आकर्षण में भी श्वास-प्रश्वास ही की क्रिया देखी। पशुओं से मनुष्य की श्रेष्ठता की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की कि मनुष्य सिर ऊंचा करके श्वास लेता है, इसलिए वह पवित्रतर वायु ग्रहण करता है।
--------------------------------------------------------------
1. जी. एच. ल्यूस-दर्शन का जीवनीमय इतिहास, पृ.9
ऐनाक्सिमिन्डेर (जन्म ई. पू. 610) एक गणितज्ञ थे। उन्होंने थेलिस के जल वाले सिद्धांत पर आपत्ति की और यह कहा कि जल तो एक वस्तु मात्र है और एक वस्तु सब वस्तु नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संसार की उत्पत्ति जल से नहीं बल्कि सीमाहीन अखिल से हुई। यद्यपि सीमाहीन अखिल संबंधी उनकी धारणा बहुत कुछ सूक्ष्म है, फिर भी वह एक बड़ी हद तक पादार्थिक है। सीमाहीन अखिल से उनका मतलब किसी निराकार धारणा से नहीं बल्कि सब वस्तुओं से था। उन्होंने उसे एक विचार या प्रतीक तक पहुंचा नहीं दिया था जैसाकि ल्यूस ने लिखा है : ‘‘उनकी सर्ववस्तु की धारणा असीम अस्तित्व की है न कि असीम मन की।’’ दूसरे शब्दों में, हम ऐनाक्सिमिन्डेर को भी भाववादी नहीं कह सकते।
पाईथागोरस को इसके बाद गिना जाता है यद्यपि उनका काल ठीक-ठीक ज्ञात नहीं। विभिन्न हिसाबों के अनुसार उनकी काल-गणना में 84 साल का अंतर पड़ता है। उनके संबंध में यह कहा जाता है कि फिलॉसफी या दर्शन शब्द का प्रयोग पहले-पहल उन्होंने ही किया। यहां भारतीय पाठक के लिए एक दिलचस्पी की बात यह है कि उनके संबंध में यह जनश्रुति है कि उनके बड़प्पन का कारण प्राच्य शिक्षा थी। पर प्राच्य शब्द से क्या मतलब है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वे फिलॉसफी शब्द से क्या अर्थ लेते थे, यह भी स्पष्ट कर दिया जाए। उन्होंने लियोन्टियस से कहा था, ‘मुझेमें कोई कला नहीं है, मैं तो फिलॉसफर (दार्शनिक) हूं।’’
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा था, ‘‘दार्शनिक वही है जो लोभ और अहंकार त्याग कर प्रकृति का अध्ययन करता है।’’ यह तो स्पष्ट है कि दर्शन से उनका मतलब मेटाफिजिक्स या ऐसी बातों पर दंतकटाकटी करना नहीं था, जो अप्रमेय हों। उन्होंने एक गुप्त समिति भी बनाई थी, जिसमें बड़ी गंभीर परीक्षाओं के बाद ही किसी को लिया जाता था। पांच साल तक तो अभ्यर्थी या उम्मीदवार को मौन धारण करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कृच्छ साधन कराए जाते थे। इन परीक्षाओं के बाद प्रार्थी को गणित से आरंभ करना पड़ता था क्योंकि गणित के संबंध में यह समझा जाता था कि यह शरीर और शरीरी वस्तुओं के बीच एक माध्यम के रूप में काम करते हुए इंटेलिजिबिल यानी बौद्धिक वस्तुओं में ही जा सकता है।
पाईथागोरस की शिक्षा यह थी कि संख्या ही वस्तुओं का मूलतत्व है। उनका कहना था कि प्रत्येक वस्तु बराबर स्थिति और गुण बदल रही है, इसका कारण परिवर्तनीय है पर अस्तित्व का मूलतत्त्व परिवर्तनीय नहीं हो सकता। पाईथागोरस का कहना यह था कि इस परिवर्तनशीलता और विविधता की तह में कोई न कोई अपरिवर्तनीय अस्तित्व होगा, इसी का नाम उन्होंने संख्या रखा। उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक वस्तु की स्थिति, गुण आदि में परिवर्तन हो सकता। उनका कहना था कि यह हमेशा ‘एक’ वस्तु रहेगी, किसी भी रूप में इस एकत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। यह न तो एक से बढ़ सकता है, न अनेक हो सकता है। यदि उसे तोड़ा जाए, तो भी वह एक ही रहेगा।
कहना न होगा कि यह विचार-पद्धति बहुत कुछ अद्भुत है क्योंकि किसी भी तरह एक शब्द को ला देने से ही इसे सार्थकता प्राप्त होती है। जो कुछ भी हो, इसी प्रकार तर्क करते हुए उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अनंत की संज्ञा एक ही है। उन्होंने कहा कि ‘एक’ निरवच्छिन्न संज्ञा है जिसे किसी और वस्तु से, यहां तक कि किसी और संख्या से, संबंध की आवश्यकता नहीं है। दो का अर्थ एक और एक है। इसी प्रकार सारी संख्याएं हैं। इन बातों से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गयी है कि पाईथागोरस एकेश्वरवादी थे। पर इस प्रकार की धारणा का कोई अर्थ नहीं मालूम होता क्योंकि वहां तो केवल ‘एक’ है, ईश्वर का कहीं पता नहीं; और वह एक किस प्रकार है, उसका कुछ दिग्दर्शन नहीं कराया गया।
जेनोफेनिस (जन्म लगभग ई. पू. 620) ने एकेश्वरवाद की बातें कहीं, पर उनके एकेश्वरवाद में विश्व, संसार और ईश्वर की एकता अंतर्निहित थी। वे विश्व, संसार और ईश्वर को पृथक करने देखने में असमर्थ थे।
हेराक्लिटस (जन्म ई. पू. 503) अग्नि से विश्व की उत्पत्ति मानते थे। उनका कहना था कि इस विश्व की रचना न ईश्वर ने की है, न मनुष्य ने, यह था, है, और हमेशा एक चिरंजीवी अग्नि के रूप में रहेगा, जो उचित प्रमाण में आत्म-निर्वासित है। उन्होंने इसी के साथ परिवर्तन के सिद्धांत को भी संयुक्त कर दिया क्योंकि आग तो हमेशा, जलती, लपटें देती, राख बनाती रहती है।
ऐम्पेडोक्लिस (जन्म लगभग ई. पू. 444) ने यह कहा कि चार मूल तत्व हैं–क्षिति, अप्, तेज और मरुत्। उनको बुद्धि और प्रयोग में संदेह था।
डिमोक्रिटस (जन्म ई. पू. 460) बहुत धनी परिवार के थे। कहा जाता है कि उन्हें मिस्र में भ्रमण करने का मौका मिला और उससे उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने एक तत्व या चार तत्वों के सिद्धांत का त्याग कर दिया और कहा कि परमाणु से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। स्मरण रहे कि उनका परमाणु सिद्धांत आधुनिक परमाणु सिद्धांत से पृथक था।
प्रोटागोरस डिमोक्रिटस के ही समसामयिक थे। उन्होंने यह सिद्धांत रखा कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का पैमाना है। उन्होंने यह कहा कि भूत बदलते रहते हैं, उम्र तथा अवस्था के अनुसार अनुभूतियां भी बदलती रहती हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों की अनुभूतियों में भी फर्क होता है। इसलिए मनुष्य ही मानदंड है। जो कुछ मनुष्य अनुभव करता है, वह है। बाकी का अस्तित्व नहीं है।
ग्रीक दार्शनिक सुकरात का समय लगभग ई. पू. 441 से 399 के बीच समझा जाता है। संसार के इतिहास में बहुत थोड़े से लोग ऐसे हुए, जिनके व्यक्तित्व और जीवन का अपने बाद के लोगों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा।
सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, पर उनके शिष्यों ने उन पर बहुत लेख लिखे और उसी के आधार पर हमारे सामने सुकरात का व्यक्तित्व उभरता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सुकरात के विचारों का महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि उन्होंने पहले-पहल परंपरा से हटकर, बिल्कुल उससे ऊपर उठकर सत्य की खोज करने की आवाज दी। यह उस युग में ही नहीं बल्कि आज के युग में भी बहुत बड़ी आवाज है और यह नहीं कहा जा सकता कि आज इस प्रकार के चिंतन या नारे की आवश्यकता नहीं है।
सुकरात के समय में कुछ फिरके, संप्रदाय ऐसे थे, जिनकी बातों को लोग बिना सोचे-विचारे मान लिया करते थे। उन्हीं बातों को जानना उस समय विद्या कहलाती थी। दुख है, उनके लगभग ढाई हजार वर्ष बाद परंपराएं और आंधविश्वास आज भी सत्य के मार्ग को संपूर्ण रूप से अवरुद्ध किए हुए हैं। हमारे यहां तो मुसीबत यह है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ लोगों के आचरण में कोई फर्क नहीं आता मानों ज्ञान का आयाम और हो, जीवन जीने का आयाम और हो। जब लोगों को सूर्य-ग्रहण या चंद्र-ग्रहण के संबंध में कुछ पता नहीं था और वे मात्र अनुमान और अटकल से सहारे चलते थे, उस युग में लोगों ने कुछ कल्पनाएं की थीं। हां, कुछ कल्पनाएं कवित्वपूर्ण हो गयीं; जैसे समुद्रमंथन। पर आज भी उन्हीं अटकलों और गपोड़ों को आधार बनाकर ग्रहण के अवसर पर राहु और केतु से चंद्र और सूरज की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, फिर मोक्ष स्नान करना–यह समझ में नहीं आता। इस समय लगभग बीस प्रतिशत व्यक्ति अपनी स्कूली किताबों में यह पढ़ते हैं कि चंद्र-ग्रहण या सूर्य-ग्रहण कैसे होता है ? इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि लोग जानते नहीं हैं। फिर भी ग्रहणों के अवसरों पर विशेष दान देना और स्नान आदि करना जारी है। ये दोनों काम अच्छे हैं, पर उन्हें पहले के अज्ञान के साथ संयुक्त करके जारी रखना यही तो समस्या है।
सुकरात के युग में रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करना और लोगों से विद्रोह की बात कहना, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए सुकरात को विष का प्याला पिलाकर मृत्यु-दंड दिया गया। सुकरात ने जिन कुसंस्कारों के साथ लड़ाई की, आज वे कुसंस्कार उसी रूप में मौजूद नहीं हैं। फिर भी, जैसा कि मैंने बताया, अंधविश्वास और कुसंस्कारों की आज भी कमी नहीं है और हमने यह भी देख लिया कि ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ स्वयं कुसंस्कारों का अंत नहीं होता। यह स्थिति बहुत अद्भुत है। इसी कारण आज भी सुकरात की उतनी ही आवश्यकता है।
हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार जर्मन महाकवि गेटे ने कालिदास के शकुंतला नाटक की प्रशंसा की है, पर ग्रीस के कवियों के संबंध में उनके ये मंतव्य विशेष ध्यान देने योग्य हैं। उनका कहना है : ‘‘इशीलस और सोफोक्लिस की तरह प्राचीन ग्रीक कवियों के सामने मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं हूं।’’
कवि वर्डसवर्थ ने इसी प्रकार कहा है : ‘‘भला डिमोस्थिनिस से बढ़कर वक्ता और शेक्सपियर के बाद इशीलस-सोफोक्लिस (यूरिपिडिस का तो कुछ कहना ही नहीं) के मुकाबले में काव्यमय नाटक कहां मिल सकते हैं ।’’
हेरोडोटस से संबंध में वर्डसवर्थ का यह कहना था कि बाइबिल के बाद उससे बढ़कर दिलचस्प और शिक्षाप्रद कोई पुस्तक नहीं है। कविवर शैली की प्रशंसा इनके मुकाबले में कम उच्छ्वसित थी, पर उनका भी यह कहना था : ‘‘ग्रीकों की कविता दूसरे साहित्यों के मुकाबले में काफी ऊंचा मानदंड रखती है, यद्यपि वह इतनी ऊंची नहीं है कि वह बहुत ऊंची जंचे और दूसरी बहुत नीचे।’’
उनका कहना था, ‘‘पैरिक्लिस के जन्म और अरस्तू की मृत्यु के बीच का युग निश्चित रूप से विश्व-इतिहास का सबसे स्मरणीय युग है। चाहे इस पर अलग से विचार किया जाए या बाद के सभ्य मानव पर उसका क्या असर रहा, उस दृष्टि से उस पर विचार किया जाए।... इन सूक्ष्म और गंभीर मनों के जो इतस्ततः विक्षिप्त टुकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, वे सुंदर मूर्ति के भग्नांशों की तरह हमारे सामने अस्पष्ट रूप से उस समय की महत्ता तथा पूर्णता का चित्र पेश करते हैं जो अब नहीं रहा। विविधता, सरलता, नमनीयता, प्रचुरता, जिस दृष्टि से भी देखा जाए, पाश्चात्य जगत में ग्रीक भाषा से बढ़कर कोई भाषा न रही।’’
इसी प्रकार सैकड़ों उद्धरण दिए जा सकते हैं। फ्रांस के युगांतरकारी लेखक अनातोल फ्रांस का यह वक्तत्व्य सुनिए : ‘‘मैं अब जानता हूं कि मैं ग्रीकों का कितना ऋणी हूं क्योंकि मेरा सब कुछ उन्हीं का है। हम जानते हैं जगत और मनुष्य का जो कुछ भी बुद्धिसंगत है, वह सब उन्हीं से आया हुआ है।’’
मिल का तो यह कहना था कि ईसाइयत के अतिरिक्त बाकी सभी ऐसी चीजों की उत्पत्ति, जिन पर आधुनिक जगत नाज करता है, ग्रीस से हुई। और उद्धरणों को आवश्यकता नहीं है।
हम सुकरात के पहले के ग्रीक दर्शन-शास्त्र पर एक विहंगम दृष्टि डाल लें। थेलस या थेलिस को ग्रीक दर्शन का पिता बताया गया है। उनका जन्म ई. पू. 626 में एशियाई कोचक के मिलिटस नामक स्थान में हुआ था। इनका कहना था कि जल ही मौलिक उपादान है और उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि आर्द्रता एक ऐसा उपादान है, जो सब में परिव्याप्त है। इस प्रकार से वे भौतिकवादी थे, क्योंकि वे जल से ही जगत की उत्पत्ति मानते थे। मजे की बात यह है कि वे देवताओं को भी मानते थे, पर साथ ही यह भी बताते थे कि उत्पत्ति भी जल से ही हुई है।
ऐनैक्सिमिनिस नामक दार्शनिक भी मिलिटस में पैदा हुए थे। उनका जन्म ई. पू. 529 या ई. पू. 548 में हुआ। वे सब चीजों की उत्पत्ति वायु से मानते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि उनके अंदर जो वायु है, वही उन्हें चला रही है और यही जीवन है। उन्होंने इस प्रकार तर्क किया कि भीतर की वायु बाहर की वायु का ही अंग है, इसलिए सब चीजों की उत्पत्ति वायु से ही हुई। इस प्रकार ऐनैक्सिमिनिस भी भौतिकवादी रहे।
पर उनके अनुयायी ऐपोलोनिया के डोयोजिनिस ने एक नया मोड़ दिया और भाववाद का प्रारंभ किया। डोयोजिनिस ने ऐनैक्सिमिनिस के अनुसार वायु को ही प्रथम माना। पर उन्होंने वायु को एक विस्तृतर और गंभीरतर अर्थ दिया, जिसमें वह करीब-करीब आत्मा हो गयी। उन्होंने इसे शक्ति और बुद्धि से समन्वित करके कल्पना की। उन्होंने यह भी कहा कि यह विश्व एक सप्राण अस्तित्व है, जो स्वतःस्फूर्त रूप से अपना विकास कर रहा है और इसमें जो कुछ परिवर्तन हो रहा है, वह उसकी जीवनी-शक्ति के कारण हो रहा है।1 उनका कहना यह था कि सारी सृष्टि और पादार्थिक क्रिया श्वास-प्रश्वासमूलक है। उन्होंने आर्द्रता के प्रति सूर्य के आकर्षण और लोहे के प्रति चुंबक के आकर्षण में भी श्वास-प्रश्वास ही की क्रिया देखी। पशुओं से मनुष्य की श्रेष्ठता की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार की कि मनुष्य सिर ऊंचा करके श्वास लेता है, इसलिए वह पवित्रतर वायु ग्रहण करता है।
--------------------------------------------------------------
1. जी. एच. ल्यूस-दर्शन का जीवनीमय इतिहास, पृ.9
ऐनाक्सिमिन्डेर (जन्म ई. पू. 610) एक गणितज्ञ थे। उन्होंने थेलिस के जल वाले सिद्धांत पर आपत्ति की और यह कहा कि जल तो एक वस्तु मात्र है और एक वस्तु सब वस्तु नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि संसार की उत्पत्ति जल से नहीं बल्कि सीमाहीन अखिल से हुई। यद्यपि सीमाहीन अखिल संबंधी उनकी धारणा बहुत कुछ सूक्ष्म है, फिर भी वह एक बड़ी हद तक पादार्थिक है। सीमाहीन अखिल से उनका मतलब किसी निराकार धारणा से नहीं बल्कि सब वस्तुओं से था। उन्होंने उसे एक विचार या प्रतीक तक पहुंचा नहीं दिया था जैसाकि ल्यूस ने लिखा है : ‘‘उनकी सर्ववस्तु की धारणा असीम अस्तित्व की है न कि असीम मन की।’’ दूसरे शब्दों में, हम ऐनाक्सिमिन्डेर को भी भाववादी नहीं कह सकते।
पाईथागोरस को इसके बाद गिना जाता है यद्यपि उनका काल ठीक-ठीक ज्ञात नहीं। विभिन्न हिसाबों के अनुसार उनकी काल-गणना में 84 साल का अंतर पड़ता है। उनके संबंध में यह कहा जाता है कि फिलॉसफी या दर्शन शब्द का प्रयोग पहले-पहल उन्होंने ही किया। यहां भारतीय पाठक के लिए एक दिलचस्पी की बात यह है कि उनके संबंध में यह जनश्रुति है कि उनके बड़प्पन का कारण प्राच्य शिक्षा थी। पर प्राच्य शब्द से क्या मतलब है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। वे फिलॉसफी शब्द से क्या अर्थ लेते थे, यह भी स्पष्ट कर दिया जाए। उन्होंने लियोन्टियस से कहा था, ‘मुझेमें कोई कला नहीं है, मैं तो फिलॉसफर (दार्शनिक) हूं।’’
इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने कहा था, ‘‘दार्शनिक वही है जो लोभ और अहंकार त्याग कर प्रकृति का अध्ययन करता है।’’ यह तो स्पष्ट है कि दर्शन से उनका मतलब मेटाफिजिक्स या ऐसी बातों पर दंतकटाकटी करना नहीं था, जो अप्रमेय हों। उन्होंने एक गुप्त समिति भी बनाई थी, जिसमें बड़ी गंभीर परीक्षाओं के बाद ही किसी को लिया जाता था। पांच साल तक तो अभ्यर्थी या उम्मीदवार को मौन धारण करना पड़ता था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से कृच्छ साधन कराए जाते थे। इन परीक्षाओं के बाद प्रार्थी को गणित से आरंभ करना पड़ता था क्योंकि गणित के संबंध में यह समझा जाता था कि यह शरीर और शरीरी वस्तुओं के बीच एक माध्यम के रूप में काम करते हुए इंटेलिजिबिल यानी बौद्धिक वस्तुओं में ही जा सकता है।
पाईथागोरस की शिक्षा यह थी कि संख्या ही वस्तुओं का मूलतत्व है। उनका कहना था कि प्रत्येक वस्तु बराबर स्थिति और गुण बदल रही है, इसका कारण परिवर्तनीय है पर अस्तित्व का मूलतत्त्व परिवर्तनीय नहीं हो सकता। पाईथागोरस का कहना यह था कि इस परिवर्तनशीलता और विविधता की तह में कोई न कोई अपरिवर्तनीय अस्तित्व होगा, इसी का नाम उन्होंने संख्या रखा। उन्होंने यह कहा कि प्रत्येक वस्तु की स्थिति, गुण आदि में परिवर्तन हो सकता। उनका कहना था कि यह हमेशा ‘एक’ वस्तु रहेगी, किसी भी रूप में इस एकत्व में परिवर्तन नहीं हो सकता। यह न तो एक से बढ़ सकता है, न अनेक हो सकता है। यदि उसे तोड़ा जाए, तो भी वह एक ही रहेगा।
कहना न होगा कि यह विचार-पद्धति बहुत कुछ अद्भुत है क्योंकि किसी भी तरह एक शब्द को ला देने से ही इसे सार्थकता प्राप्त होती है। जो कुछ भी हो, इसी प्रकार तर्क करते हुए उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि अनंत की संज्ञा एक ही है। उन्होंने कहा कि ‘एक’ निरवच्छिन्न संज्ञा है जिसे किसी और वस्तु से, यहां तक कि किसी और संख्या से, संबंध की आवश्यकता नहीं है। दो का अर्थ एक और एक है। इसी प्रकार सारी संख्याएं हैं। इन बातों से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गयी है कि पाईथागोरस एकेश्वरवादी थे। पर इस प्रकार की धारणा का कोई अर्थ नहीं मालूम होता क्योंकि वहां तो केवल ‘एक’ है, ईश्वर का कहीं पता नहीं; और वह एक किस प्रकार है, उसका कुछ दिग्दर्शन नहीं कराया गया।
जेनोफेनिस (जन्म लगभग ई. पू. 620) ने एकेश्वरवाद की बातें कहीं, पर उनके एकेश्वरवाद में विश्व, संसार और ईश्वर की एकता अंतर्निहित थी। वे विश्व, संसार और ईश्वर को पृथक करने देखने में असमर्थ थे।
हेराक्लिटस (जन्म ई. पू. 503) अग्नि से विश्व की उत्पत्ति मानते थे। उनका कहना था कि इस विश्व की रचना न ईश्वर ने की है, न मनुष्य ने, यह था, है, और हमेशा एक चिरंजीवी अग्नि के रूप में रहेगा, जो उचित प्रमाण में आत्म-निर्वासित है। उन्होंने इसी के साथ परिवर्तन के सिद्धांत को भी संयुक्त कर दिया क्योंकि आग तो हमेशा, जलती, लपटें देती, राख बनाती रहती है।
ऐम्पेडोक्लिस (जन्म लगभग ई. पू. 444) ने यह कहा कि चार मूल तत्व हैं–क्षिति, अप्, तेज और मरुत्। उनको बुद्धि और प्रयोग में संदेह था।
डिमोक्रिटस (जन्म ई. पू. 460) बहुत धनी परिवार के थे। कहा जाता है कि उन्हें मिस्र में भ्रमण करने का मौका मिला और उससे उन्हें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने एक तत्व या चार तत्वों के सिद्धांत का त्याग कर दिया और कहा कि परमाणु से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। स्मरण रहे कि उनका परमाणु सिद्धांत आधुनिक परमाणु सिद्धांत से पृथक था।
प्रोटागोरस डिमोक्रिटस के ही समसामयिक थे। उन्होंने यह सिद्धांत रखा कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का पैमाना है। उन्होंने यह कहा कि भूत बदलते रहते हैं, उम्र तथा अवस्था के अनुसार अनुभूतियां भी बदलती रहती हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ व्यक्तियों की अनुभूतियों में भी फर्क होता है। इसलिए मनुष्य ही मानदंड है। जो कुछ मनुष्य अनुभव करता है, वह है। बाकी का अस्तित्व नहीं है।
ग्रीक दार्शनिक सुकरात का समय लगभग ई. पू. 441 से 399 के बीच समझा जाता है। संसार के इतिहास में बहुत थोड़े से लोग ऐसे हुए, जिनके व्यक्तित्व और जीवन का अपने बाद के लोगों पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा।
सुकरात ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखा, पर उनके शिष्यों ने उन पर बहुत लेख लिखे और उसी के आधार पर हमारे सामने सुकरात का व्यक्तित्व उभरता है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से सुकरात के विचारों का महत्व इसलिए बहुत अधिक है कि उन्होंने पहले-पहल परंपरा से हटकर, बिल्कुल उससे ऊपर उठकर सत्य की खोज करने की आवाज दी। यह उस युग में ही नहीं बल्कि आज के युग में भी बहुत बड़ी आवाज है और यह नहीं कहा जा सकता कि आज इस प्रकार के चिंतन या नारे की आवश्यकता नहीं है।
सुकरात के समय में कुछ फिरके, संप्रदाय ऐसे थे, जिनकी बातों को लोग बिना सोचे-विचारे मान लिया करते थे। उन्हीं बातों को जानना उस समय विद्या कहलाती थी। दुख है, उनके लगभग ढाई हजार वर्ष बाद परंपराएं और आंधविश्वास आज भी सत्य के मार्ग को संपूर्ण रूप से अवरुद्ध किए हुए हैं। हमारे यहां तो मुसीबत यह है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ लोगों के आचरण में कोई फर्क नहीं आता मानों ज्ञान का आयाम और हो, जीवन जीने का आयाम और हो। जब लोगों को सूर्य-ग्रहण या चंद्र-ग्रहण के संबंध में कुछ पता नहीं था और वे मात्र अनुमान और अटकल से सहारे चलते थे, उस युग में लोगों ने कुछ कल्पनाएं की थीं। हां, कुछ कल्पनाएं कवित्वपूर्ण हो गयीं; जैसे समुद्रमंथन। पर आज भी उन्हीं अटकलों और गपोड़ों को आधार बनाकर ग्रहण के अवसर पर राहु और केतु से चंद्र और सूरज की मुक्ति के लिए प्रार्थना करना, फिर मोक्ष स्नान करना–यह समझ में नहीं आता। इस समय लगभग बीस प्रतिशत व्यक्ति अपनी स्कूली किताबों में यह पढ़ते हैं कि चंद्र-ग्रहण या सूर्य-ग्रहण कैसे होता है ? इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि लोग जानते नहीं हैं। फिर भी ग्रहणों के अवसरों पर विशेष दान देना और स्नान आदि करना जारी है। ये दोनों काम अच्छे हैं, पर उन्हें पहले के अज्ञान के साथ संयुक्त करके जारी रखना यही तो समस्या है।
सुकरात के युग में रूढ़ियों और परंपराओं के विरुद्ध विद्रोह करना और लोगों से विद्रोह की बात कहना, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसीलिए सुकरात को विष का प्याला पिलाकर मृत्यु-दंड दिया गया। सुकरात ने जिन कुसंस्कारों के साथ लड़ाई की, आज वे कुसंस्कार उसी रूप में मौजूद नहीं हैं। फिर भी, जैसा कि मैंने बताया, अंधविश्वास और कुसंस्कारों की आज भी कमी नहीं है और हमने यह भी देख लिया कि ज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ स्वयं कुसंस्कारों का अंत नहीं होता। यह स्थिति बहुत अद्भुत है। इसी कारण आज भी सुकरात की उतनी ही आवश्यकता है।
|
|||||
लोगों की राय
No reviews for this book